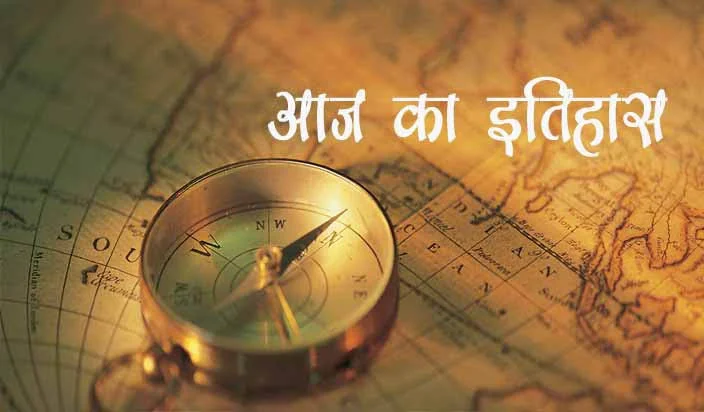संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर गठित सरकारों के पैनल (आईपीसीसी)की ताजा रिपोर्ट में भारत को लेकर निराशानजनक तस्वीर पेश की गई है। उसमें कहा गया है कि भारत अगले दो दशकों में जलवायु परिवर्तन से होने वाली बहुत सारी तबाहियों का सामना करने को विवश हो सकता है। अगर 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती नहीं की गई तो जलवायु परिवर्तन जनित विनाश को रोक पाना संभव नहीं होगा। आईपीसीसी रिपोर्ट साफतौर पर दिखाती है कि बहुत सारे जलवायु और गैर जलवायु खतरे एक-दूसरे से जुड़ेंगे और नतीजे में तमाम सेक्टरों और क्षेत्रों में तमाम किस्म के खतरों की गति को और तेज कर देंगे। भारत के सामने ये खास किस्म की चुनौतियां होंगी। भारत सरकार के लिए ये रिपोर्ट खतरे की घंटी की तरह है, उसे मुस्तैदी से निर्णय के सभी स्तरों में जलवायु चिंताओं को मुख्य जगह देनी होगी। 67 देशों के वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट तैयार की है, इनमें से नौ भारत से हैं। रिपोर्ट बताती है कि इसमें पानी की केंद्रीय भूमिका होती है। जैसे-बहुत सारे अनुकूलन अभी पानी से जुड़े नुकसानों की प्रतिक्रिया स्वरूप हो रहे हैं। दूसरी ओर दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पानी से जुड़े प्रभावों के जरिए जलवायु परिवर्तन की मार को झेल रहा है तो इस रूप में भी पानी पूरी समस्या का एक हिस्सा बना है। उल्लेखनीय है कि भारत की 40 फीसदी से ज्यादा आबादी 2050 तक पानी की किल्लत से जूझ रही होगी और उसी दौरान देश के तटीय इलाके, जिनमें मुंबई जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं, समुद्र के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित हो रहे होंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनों में और बाढ़ आएगी और उसी दौरान सूखे और पानी की किल्लत से फसल उत्पादन भी गिरेगा। भारत के लिए ये अस्तित्व का संकट है। इससे निपटने के लिए अवसर की जो खिड़की मिली है वो भी बंद हो रही हैं। रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि जलवायु परिवर्तन से भारत के शहरी इलाकों में स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी ढांचा पहले ही प्रभावित हो चुका है। 2015 और 2020 के बीच शहरों में 35 फीसदी वृद्धि हुई है। अगले 15 साल में शहरों में कम से कम 60 करोड़ और निवासी हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन की विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई की दरकार है। सरकारें, निजी सेक्टर और स्थानीय समुदाय को खतरे कम करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। हमें फौरी उपायों या तात्कालिक समाधानों से बचना होगा। असहायता और संकट के मूल कारणों को कम करने के लिए हमें रूपांतरण के स्तर पर खुद को ढालने की जरूरत है, इसके लिए तमाम प्रणालियों और व्यवस्थाओं को गैर टिकाऊ लक्ष्यों से दूर हटाना होगा। सनद रहे कि नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो जलवायु बैठक में कहा था कि भारत 2030 तक अपनी गैर-ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावॉट तक बढ़ाकर अपनी 50 फीसदी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकता है। मोदी ने ये भी कहा कि भारत 2030 तक अपने कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में भी कटौती करेगा,अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन भागीदारी को 2030 तक 45 फीसदी तक कम कर देगा और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल कर लेगा। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ऊर्जा सेक्टर के उत्सर्जनों में कटौती के लिए कदम उठा रही है। जानकारों का कहना है कि विकसित देशों को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जानना चाहिए कि अतीत में वे क्या कर गुजरे हैं। आईपीसीसी की अगली रिपोर्ट अप्रैल में आएगी। उसमें जलवायु संकट से निपटने और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के उपायों से जुड़े परामर्श दिए जाएंगे। ऐसे में भारत को अपने हित में काम करना होगा। हमारी जलवायु रणनीति सह-लाभों पर आधारित होनी चाहिए। हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय करने चाहिए क्योंकि ये दुनिया के लिए ही नहीं, हमारे अपने लिए भी यही बेहतर होगा।
जलवायु परिवर्तन