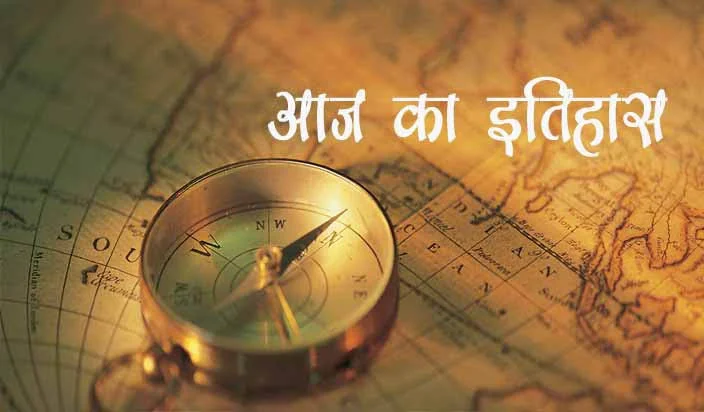रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते उत्पन्न भू-राजनीतिक तनावों ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को उलट-पलट कर दिया है। इस उथल-पुथल में भारत और चीन की नीति, खासकर रूसी तेल खरीद के मामले में उनकी ऊर्जा सुरक्षा की प्राथमिकताओं को दर्शाती है। लेकिन अब अमरीका की ओर से लगाए जा रहे सेकेंडरी प्रतिबंध और अतिरिक्त टैरिफ इस रणनीति को एक नए संकट की ओर धकेल रहे है। भारत और चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी आर्थिक संप्रभुता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए समझौता नहीं करेंगे। अमरीका की चेतावनियों और दबाव को दोनों देशों ने न केवल अस्वीकार्य बताया, बल्कि इसे एकतरफा और अनुचित करार दिया है। भारत का रुख साफ है- वह न तो किसी गुट की कठपुतली बनेगा, न ही किसी की नीति का अनुसरण करेगा, जो उसकी ऊर्जा रणनीति के विपरीत हो। भारत का रूस से तेल खरीदना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। यह उसकी बहुपक्षीय विदेश नीति और ऊर्जा के किफायती स्रोतों की खोज का हिस्सा था। जब पश्चिमी देशों ने रूस से हाथ खींचा, तो भारत को सस्ती दरों पर ऊर्जा उपलब्ध हुई। परिणामस्वरूप भारत ने न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की, बल्कि 33 अरब डॉलर तक की बचत भी की। ट्रंप प्रशासन की ओर से अब जो 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है, वह भारत पर जबरन दबाव बनाने का प्रयास है। इस कदम से न केवल भारत की तेल बिलिंग 11 अरब डॉलर तक बढ़ सकती है, बल्कि वैश्विक तेल कीमतों पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। यह विडंबना ही है कि जो अमरीका कभी भारत के रूसी तेल आयात का समर्थन कर चुका था, वही अब उसे दंडित करने की तैयारी में है। यह सवाल भी अहम है कि अगर भारत जैसे बड़े उपभोक्ता रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें कहां पहुंचेंगी? 100, 120 या 300 डॉलर प्रति बैरल? दुनिया 2022 जैसी स्थिति को फिर झेलने की स्थिति में नहीं है। उस समय भी भारत ने रूसी तेल खरीद कर एक तरह से वैश्विक कीमतों को स्थिर रखने में भूमिका निभाई थी। विशेषज्ञों की चेतावनी भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती- भारत अगर रूस के तेल बाजार से हटता है तो ओपेक की उत्पादन वृद्धि भी इस घाटे की भरपाई नहीं कर पाएगी। साथ ही भारत की कंपनियों की अमरीकी वित्तीय प्रणाली तक पहुंच खतरे में पड़ सकती है, जिससे वैश्विक निवेश और व्यापारिक संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। भारत को अब कूटनीतिक स्तर पर एक सशक्त प्रतिक्रिया की जरूरत है- न केवल अमरीका के साथ बातचीत में, बल्कि वैश्विक मंचों पर भी। इस मसले पर ऊर्जा उपभोक्ता देशों का साझा दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक हो गया है, ताकि किसी एक देश के निर्णय से वैश्विक आर्थिक अस्थिरता पैदा न हो। ऐसे में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। सेकेंडरी प्रतिबंध माहौल को और बिगाड़ सकते हैं, इससे भारतीय कंपनियों की अमरीकी वित्तीय प्रणाली तक पहुंच खतरे में पड़ सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर रूस का पांच मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन अचानक से वैश्विक बाजार से हटा दिया जाएगा, तो तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ सकता है, जिससे प्रभावित देशों को तुरंत वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ेगी और हाल ही में ओपेक द्वारा की गई उत्पादन वृद्धि भी इतनी बड़ी मात्रा की भरपाई करने के लिए काफी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उत्पादन क्षमता सीमित है। वर्तमान समय में अमरीका पूरी दुनिया की अर्थ-व्यवस्था को अपने हिसाब से ढालना चाहता है। भारत सहित विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाना उसकी तानाशाही है। रूस-यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर रूस से तेल न खरीदने का दबाव भारत और चीन दोनों पर है। अमरीका चाहता है कि ये दोनों देश रूस से तेल खरीद कर उसे मजबूत न करें। परंतु भारत और चीन को रूस से तेल खरीदने में अपनी भलाई दिखती है। खाड़ी देशों की अपेक्षा रूस से तेल खरीदना दोनों देशों के लिए लाभकारी है। ऐसे में अमरीका का इन दोनों देशों पर दबाव बनाना सही नहीं है। अमरीका आज ही नहीं बहुत पहले से तेल के नाम पर दादागिरी करते आ रहा है। इराक पर हमला और सद्दाम हुसैन को समाप्त करना तेल राजनीति का ही एक हिस्सा था। अमरीका खुद अपने तेल भंडार को बचाकर रखे हुए है और वह खाड़ी देशों से तेल खरीद कर अपना काम चलाता है। अमरीका की यह रणनीति भले ही उसके देश के लिए अच्छी हो, परंतु वैश्विक समाज ऐसी रणनीति का समर्थन नहीं करता है।
तेल का खेल