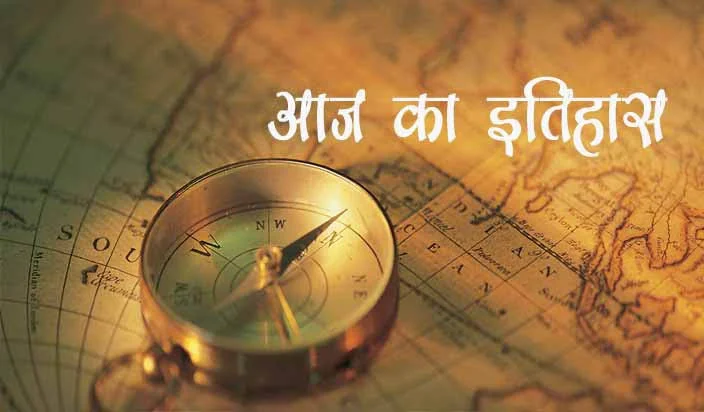पूर्वोत्तर भारत के विशाल और संवेदनशील हिमालयी भूभाग में स्थित ग्लेशियर झीलें न केवल प्राकृृतिक सुंदरता की प्रतीक हैं, बल्कि आज के दौर में एक गहराते हुए जलवायु संकट की चेतावनी भी हैं। नगालैंड विश्वविद्यालय की ओर से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ऊंंचाई पर स्थित ग्लेशियर झीलों पर किया जा रहा अध्ययन इसी चेतावनी को समझने और उसके खिलाफ समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और स्वागतयोग्य कदम है। पिछले वर्ष अक्तूबर 2023 में सिक्किम में आई विनाशकारी बाढ़, जिसने तीस्ता घाटी को झकझोर कर रख दिया ने इस बात को साफ कर दिया कि हिमालय की शांत झीलें भी जलवायु परिवर्तन की मार झेलते हुए भयावह आपदाओं का कारण बन सकती हैं। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जैसी घटनाएं अब दुर्लभ नहीं रहीं, बल्कि ये बढ़ती वैश्विक तापमान और बदलते मौसमी चक्र का सीधा नतीजा हैं। इस पृष्ठभूमि में नगालैंड विश्वविद्यालय द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, सिक्किम विश्वविद्यालय और जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट के साथ मिलकर की जा रही यह बहु-संस्थागत शोध परियोजना न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि नीति-निर्माण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी दूरगामी प्रभाव डालने वाली है। इस शोध के अंतर्गत अपनाए जा रहे बाथिमेट्रिक सर्वेक्षण और बाढ़ मॉडलिंग जैसे उन्नत उपाय, उन झीलों की गहराई, आकार और स्थिरता के बारे में निर्णायक जानकारी देंगे, जो सतह से ऊपर भले शांत नजर आएं, पर भीतर से अस्थिर हो सकती हैं। यह न केवल संभावित जोखिमों की पहचान करेगा, बल्कि स्थानीय प्रशासन को ऐसे इलाकों में पूर्व चेतावनी प्रणाली और सुरक्षा अवसंरचनाएं विकसित करने का भी आधार देगा। इस परियोजना की खास बात यह भी है कि इसके नतीजे केवल अकादमिक रिपोर्टों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इन्हें नीति-निर्माताओं, योजनाकारों और विकास से जुड़े हितधारकों के साथ साझा किया जाएगा। यह वह सेतु है जिसकी भारतीय आपदा प्रबंधन प्रणाली को सख्त आवश्यकता है - विज्ञान आधारित नीति निर्धारण। पूर्वी हिमालय, जो जैव विविधता, संस्कृृति और जल स्रोतों का अद्वितीय संगम है, आज जलवायु परिवर्तन की सबसे तीव्र मार झेल रहा है। ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, मौसम के अनिश्चित चक्र, असमय और अत्यधिक वर्षा जैसे संकेत अब चेतावनी से कहीं अधिक हैं- ये संकट की दस्तक हैं। ऐसे में यह शोध केवल भविष्य की चिंता नहीं, बल्कि वर्तमान की अनिवार्यता बन चुका है। नगालैंड विश्वविद्यालय को इस अध्ययन का नेतृत्व सौंपा जाना न केवल पूर्वोत्तर भारत की शैक्षणिक क्षमताओं पर विश्वास को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि अब जलवायु विज्ञान की 'दिल्ली-केंद्रित समझ को पर्वतीय और स्थानीय परिप्रेक्ष्य से समृद्ध करने की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर भारत में हिमालय की गोद में छिपे संकटों को उजागर करने और उन्हें समय रहते समझने का यह प्रयास सराहनीय है। आज जब देश प्राकृृतिक आपदाओं के बढ़ते जोखिम से दो-चार हो रहा है, तब ऐसी वैज्ञानिक पहलों में निवेश और सहयोग न केवल आपदाओं को रोकने का साधन है, बल्कि एक सुरक्षित, सतत और तैयार भारत की दिशा में भी मजबूत कदम है। हमें यह समझना होगा कि हिमालय केवल हमारी भौगोलिक सीमा नहीं, हमारी पारिस्थितिकीय सुरक्षा का स्तंभ भी है। उसकी रक्षा, हमारी रक्षा है - और यह रक्षा विज्ञान, नीति और संवेदनशील विकास की साझी सोच से ही संभव है।
भविष्य की तैयारी