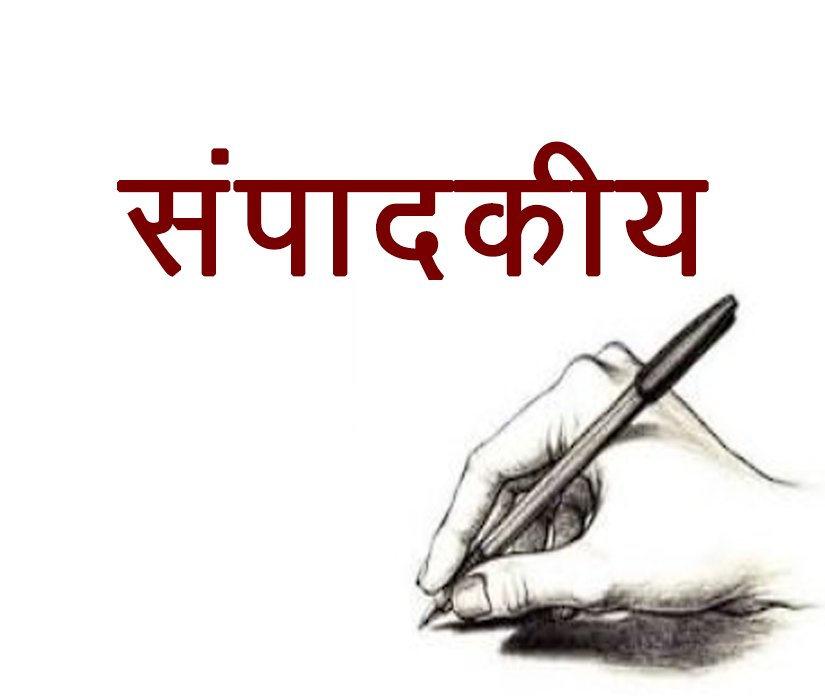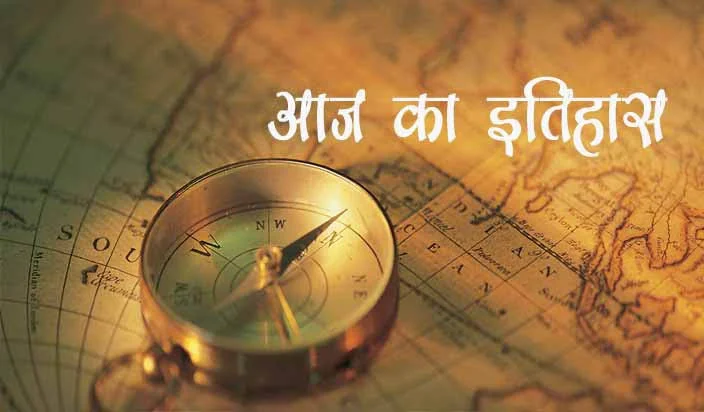कुशल श्रम को पूरी तरह से समझने के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि अकुशल श्रम का क्या अर्थ है और यह कुशल श्रम से किस प्रकार भिन्न है। अकुशल श्रम वह कार्य है जिसके लिए औपचारिक शिक्षा या किसी विशिष्ट कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। कैशियर, क्लीनर और किराना क्लर्क सभी अकुशल श्रम के उदाहरण हैं। अकुशल श्रम के बारे में सबसे आम गलतफहमियों में से एक यह है कि इसके लिए बहुत कम या बिल्कुल भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, कई मामलों में, कैशियरिंग और सफाई जैसी नौकरियों के लिए भी बहुत अधिक ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुशल श्रम वह कार्य है जिसके लिए किसी दिए गए व्यवसाय के लिए विशिष्ट तकनीकी ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। आज भारत के रोजगार क्षेत्र का एक बड़ा विरोधाभास यह है कि जहां एक ओर बेरोजगारी बड़ी चुनौती बनी हुई है, वहीं देश के संभावित बड़े नियोक्ताओं की शिकायत है कि उन्हें काम करने के लिए श्रमिक नहीं मिल रहे हैं।
गत सप्ताह लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यन ने कहा कि इंजीनियरिंग क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी को कुल मिलाकर 45,000 श्रमिकों और इंजीनियरों की जरूरत है। इस मामले में एलएंडटी कोई अपवाद नहीं है। पूरे भारत की बात करें तो पूर्व में स्टील निर्माताओं से लेकर टेक्सटाइल हब तिरुपुर तक कंपनियों को मशीन ऑपरेटर, वेल्डर, फिटर, वाहन चालक, टेक्नीशियन, कारपेंटर और प्लंबर जैसे साधारण कामों के लिए कुशल श्रमिक तलाशने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। यह कमी केवल ऑर्डर बुक के विस्तार, चुनावों या गर्मियों की वजह से नहीं है जिन्होंने श्रमिकों को वापस उनके गांव भेज दिया। यह देश के श्रम बाजार की एक पुरानी कमजोरी का परिणाम है जिसकी वजह से वेतन और लागत में ऐसे समय में इजाफा हो रहा है जब निजी क्षेत्र का निवेश अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर है। यह कमी उस समय और बढ़ जाती है जब हम मूल्य शृंखला में ऊपर जाते हैं। उस स्थिति में कंपनियों को अंतर को पाटने के लिए विदेशों खासकर चीन से तकनीशियनों और इंजीनियरों को बुलाना पड़ता है।
इस कमी की प्रमुख वजह शिक्षा और प्रशिक्षण की खराब गुणवत्ता है। इससे कंपनियों को इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ती है। ताजा इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार करीब 64 फीसदी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट रोजगार पाने योग्य हैं और इनमें से 40 फीसदी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई से आते हैं। कुल मिलाकर करीब आधे युवाओं के पास ही रोजगार पाने लायक कौशल है। दिलचस्प है कि यह हतोत्साहित करने वाली तस्वीर भी 2014 की तुलना में बेहतर है। उस समय केवल 33.9 फीसदी युवा ही रोजगार पाने लायक थे। यह सुधार सरकार के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा अप्रेंटिस एवं अन्य योजनाओं की बदौलत आया।
इस प्रगति के बावजूद रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि बाजार को कुशल श्रमिक उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यह बताती है कि केवल दो फीसदी श्रमिकों के पास औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण है और नौ फीसदी के पास अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण है। इसके अलावा सरकार के कौशल कार्यक्रमों में भी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षकों या प्रमाणन की कमी है। इसके परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित 20 फीसदी से भी कम लोगों को कंपनियों में रोजगार मिल पाया। समस्या की मूल वजह यह है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योग जगत की जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं। इससे एक बार फिर यह बात रेखांकित होती है कि उद्योग जगत के साथ करीबी भागीदारी करने की आवश्यकता है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम इस समस्या का सटीक उदाहरण हैं।
भारत हर वर्ष जो 15 लाख इंजीनियर तैयार करता है उनमें से 5 फीसदी से भी कम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों या भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों से होते हैं। अधिकांश स्नातक ऐसे निजी और सरकारी संस्थानों से आते हैं जिन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता तो होती है लेकिन उनकी गुणवत्ता में काफी अंतर होता है। सरकार द्वारा 2008 में स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एक गैर लाभकारी संस्था है जिसे उद्योग जगत के साथ काम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वह भी इस समस्या को हल नहीं कर सका।