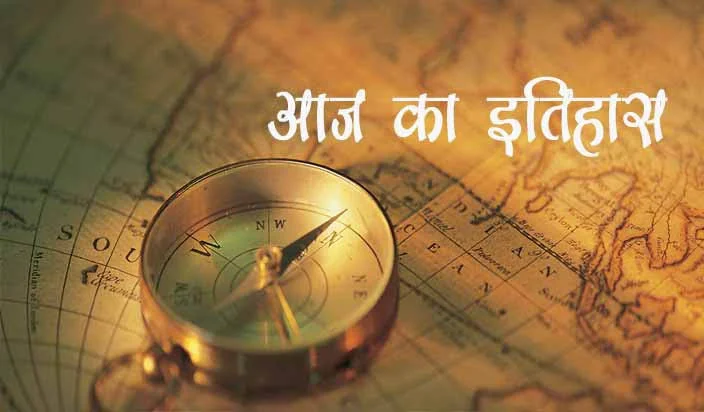इन दिनों मैट्रिक और एचएस की परीक्षाएं चल रही हैं। इस दौरान देखा जा रहा है कि बच्चे परीक्षाओं की तैयारी किताबें पढ़कर कम, मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे में स्वभाविक सवाल है कि सीखने-सिखाने के लिए बेहतर कौन है? कंप्यूटर या किताबें। सच्चाई यह है कि आज की तारीख में किसी भी विषय की जानकारी को ग्रहण करने के लिए किताब के साथ-साथ डिजिटल शिक्षा भी जरूरी है। वैसे आमतौर पर कंप्यूटरों के मुकाबले किताबें सीखने-सिखाने का बेहतरीन जरिया मानी जाती हैं। हालांकि अलग-अलग परिस्थितियों में दोनों ही बहुत उम्दा हैं। किताब बनाम कंप्यूटर की बहस शिक्षा की असल समस्या गरीबी से ध्यान भटकाती है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात ने कहा था कि चीजों को लिखने से लोग भुलक्कड़ हो जाएंगे। संयोग देखिए कि आज हम उनकी कही इस बात की चर्चा इसलिए कर पा रहे हैं कि यह बात लिखी गई थीं।
टिप्पणीकार अक्सर कहते हैं कि लिखे गए शब्दों के लिए किताबें सबसे बढ़िया माध्यम हैं और कंप्यूटर सीखने की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इन टिप्पणियों के पीछे लगभग वही कारण बताए जाते हैं, जिनके कारण सुकरात लिखने के खिलाफ थे। यह आधार था विस्मृति, यानी भूलने की प्रवृत्ति, जबकि याद रखना, सीखने की आधारशिला है। आपको हैरानी हो सकती है कि लोगों को नई तकनीकों से क्या शिकायत है? जैसे-जैसे पढ़ाई-लिखाई प्रिंट की जगह ज्यादा-से-ज्यादा डिजिटल किताबों और ऐसी अन्य चीजों की ओर बढ़ रही हैं, शोधकर्ता बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी गौर कर रहे हैं। यह क्षेत्र नया है और साक्ष्य मिले-जुले हैं। इस बात पर कोई वैज्ञानिक सहमति नहीं है कि बच्चों की शिक्षा के लिए किताबें या डिजिटल उपकरण बेहतर हैं या नहीं। उदाहरण के लिए होंडुरास के प्राथमिक विद्यालयों में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि पाठ्यपुस्तकों की जगह लैपटॉप का इस्तेमाल करने से छात्रों के सीखने में कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब, यह न तो सकारात्मक था और न ही नकारात्मक, लेकिन क्या यह सामान्य ज्ञान की बात नहीं है कि सीखने के दोनों रूप यानी प्रिंट और डिजिटल, व्यक्ति और स्थिति के आधार पर प्रभावी हो सकते हैं या नहीं? प्रारंभिक शिक्षा दिमाग मजबूत करती है इस विषय पर बात करने से पहले न्यूरो साइंस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इसके जरिए शिक्षकों को यह चुनाव करने में मदद मिल सकती है कि बच्चों के विकास के विभिन्न चरणों में कौन से उपकरण प्रयोग में लाए जाएं। तंत्रिका वैज्ञानिकों ने हमें दिखाया है कि सीखना और स्मृति का निर्माण मस्तिष्क को मजबूत और बेहतर बनाता है।
मस्तिष्क प्लास्टिक की तरह है। जैसे-जैसे हम यादें करते हैं, सीखते और भूल जाते हैं, यह बढ़ता है और न्यूरॉन्स के बीच संबंधों को काटता है। ऐसा हर उम्र में होता है, लेकिन बचपन में मस्तिष्क विशेष रूप से प्लास्टिक जैसा होता है। मस्तिष्क का यह लचीलापन काफी हद तक हमारे अनुभवों और वातावरण पर निर्भर करता है। अध्ययनों से पता चला है कि बचपन में हमारे सीखने का माहौल जितना समृद्ध होता है, हम उतनी ही ज्यादा चीजें सीख लेते हैं। जीवन भर हमारा दिमाग जिस तरह नई चीजें सीखेगा, हम उन तौर-तरीकों को भी बदलते हैं। यहां सबसे अच्छा उदाहरण भाषा सीखना है। बच्चे, वयस्कों की तुलना में दूसरी भाषा बहुत आसानी से सीखते हैं क्योंकि उनका मस्तिष्क अधिक लचीला होता है। इसके अलावा, जो वयस्क बचपन में दो भाषाएं सीखते हैं, वे उन वयस्कों की तुलना में तीसरी भाषा बहुत तेजी से सीख सकते हैं, जिन्होंने बचपन में केवल एक भाषा सीखी है। इसकी वजह यह है कि उनके दिमाग को भाषाएं सीखने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, वहीं अगर बचपन में मस्तिष्क का इस्तेमाल कम होगा, यानी सीखने की प्रक्रिया कमजोर होगी, तो ऐसी स्थिति मस्तिष्क को स्थायी रूप से बदतर या कमजोर बना देती है।
तमाम अनुभवों से वंचित बच्चों के मस्तिष्क का तुलनात्मक रूप से उतना विकास नहीं हो पाता, जितना कि अनुभवों की दुनिया में रहने वाले बच्चों का होता है। उदाहरण के लिए यदि बच्चों का वयस्कों के साथ संपर्क और बातचीत कम हो, तो उनके मस्तिष्क का विकास कम हो पाता है। ये ऐसे बदलाव हैं, जिन्हें आगे चलकर बदलना अक्सर मुमकिन नहीं हो पाता। शिक्षा के लिए इन सब बातों का क्या मतलब है? बच्चों को यथासंभव डिजिटल और भौतिक दोनों प्रकार के शिक्षण उपकरणों से अवगत कराया जाना चाहिए। दोनों का होना आज के समय की सबसे अधिक जरूरत है। इसका मतलब किसी चीज की स्थायी जानकारी के लिए किताबों और लिखावट दोनों का सहारा लिया जा सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि लिखने की क्रिया के लिए मस्तिष्क को नोट लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होने की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शिक्षा ग्रहण करने की पद्धति बदल रही है, इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रही है।