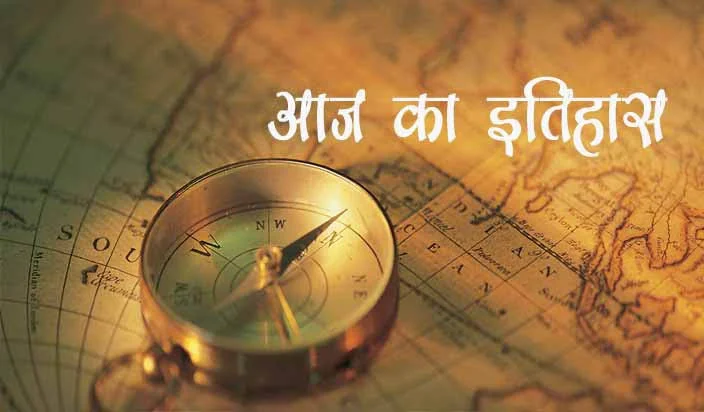इन दिनों चुनाव जीतकर सत्ता के लिए महज जादुई अंक हासिल कर लेना ही काफी नहीं है। कारण कि दूसरी पार्टी कब आपके विधायकों को तोडक़र अपने साथ जोड़ ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिलवक्त महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यूं तो विधायकों का दल बदलना भारत में कोई नई बात नहीं है, बल्कि इस समस्या से निपटने के लिए देश में दल-बदल विरोधी कानून 1985 में ही लाया गया था। उससे भी पहले 1967 में हरियाणा में गया लाल नाम के विधायक ने एक ही दिन में तीन बार पार्टी बदल कर आया राम, गया राम के मुहावरे को जन्म दिया था। 1967 से 71 के बीच 142 बार सांसदों ने और 1,969 बार अलग-अलग विधान सभाओं में विधायकों ने दल बदले। महज इन चार सालों में 32 सरकारें गिरीं यानी दल बदल कर विधायिकाओं में संवैधानिक संकट पैदा करने की परिपाटी दशकों पुरानी है,लेकिन अब इस तरह की घटनाओं की आवृत्ति बढ़ गई है। मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने से ठीक पहले भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए थे। वजह थी कांग्रेस के विधायकों का अपनी ही पार्टी के खिलाफ बागी हो जाना। उससे पहले नवंबर 2019 में कर्नाटक में भी कांग्रेस के विधायकों की ही बगावत के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी और बाद में कांग्रेस की सरकार गिर ही गई। जुलाई 2020 में राजस्थान में भी ऐसी ही उठापटक देखने को मिली,लेकिन कांग्रेस किसी तरह बागी विधायकों को वापस ले आई और राज्य में अपनी सरकार को गिरने से बचा लिया। उस प्रकरण में भी राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को हस्तक्षेप करना पड़ा था। बार-बार इस तरह विधायकों का दल बदलना उनका लोभ और पार्टियों में सत्ता का लालच दिखाता है। हालांकि कोई भी विधायक लोभ के आरोप को स्वीकार नहीं करता है। हम अक्सर विधायकों को कहते हुए पाएंगे कि वो अपनी पार्टी का दामन छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल इसलिए हो गए क्योंकि उनके हिसाब से उनकी पुरानी पार्टी अपने लक्ष्यों से भटक गई थी। दोनों पार्टियों की विपरीत विचारधारा की विसंगति पर कोई विधायक प्रकाश नहीं डालता। दल बदल के इस नए दौर के संभवत: यही मायने हैं कि भारत में राजनीति में विचारधारा नेपथ्य में चली गई है। राजनेताओं के लिए पार्टियों के बीच की सीमा लांघना कोई दुविधा का विषय नहीं रह गया है। कोई भी नेता किसी भी दिन किसी भी पार्टी में जा सकता है, कोई भी पार्टी किसी भी दिन किसी भी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन जोड़ सकती है और तोड़ भी सकती है। विचारधारा की राजनीति के कमजोर होने का समाज पर क्या असर पड़ा है, यह तो राजनीतिशास्त्रियों और सामाजशास्त्रियों के लिए अध्ययन का विषय है,लेकिन लोकतंत्र के लिए इसके मायने स्पष्ट हैं। याद कीजिए आपने पिछली बार कब मतदान किया था। अपना वोट किसको देना है ये किसी न किसी आधार पर तो तय किया होगा। चुनाव जीतने के बाद अगर उम्मीदवार की सोच में बदलाव आ जाए और वो उन सब बातों से मुकर जाए जिनसे संतुष्ट होकर आपने उसे वोट दिया था तो आपको कैसा लगेगा। विशेष रूप से चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलना एक तरह की ठगी है, मतदाता के साथ धोखाधड़ी है। इसी पर लगाम लगाने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। लेकिन स्पष्ट है कि वह कानून बुरी तरह से असफल हो चुका है। ऐसे में कैसे यह परिपाटी रुकेगी और कैसे चुनावी लोकतंत्र की शुचिता बढ़ेगी,इस सवाल का जवाब खोजने की जरूरत है। फिलहाल महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हो रहा है। सत्ता के शाह-मात खेल में एक ओर राजनीतिक पार्टियां विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने में लगी हुई हंै तो दूसरी ओर अंतिम समय में अदालत क्या फैसला सुनाती है,उस पर भी नजर है। कुल मिलाकर वर्तमान समय में महज सत्ता हासिल करने के लिए जो भी हो रहा है, वह दलीय राजनीति व उसकी वफादारी के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में दल-बदल को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की जरूरत है।
सत्ता की राजनीति