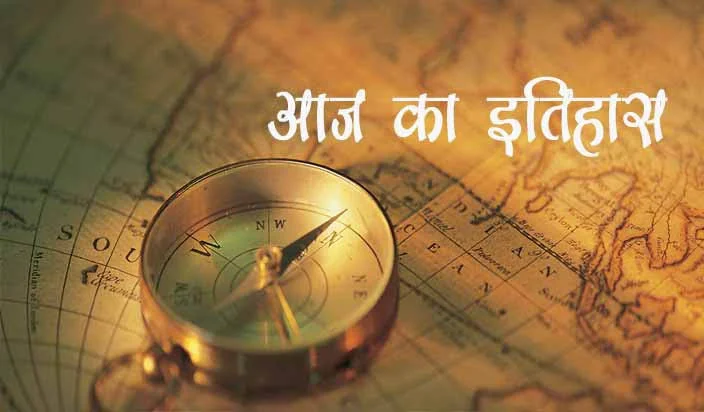बीजिंग में हाल ही में संपन्न हुआ यूरोपीय संघ (ईयू) और चीन का द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन इस बात की गवाही देता है कि वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य अब सरल समीकरणों का नहीं रहा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेय लाएन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यह बहुप्रतीक्षित बैठक जहां जलवायु परिवर्तन जैसे साझा हितों पर आंशिक सहमति लेकर समाप्त हुई, वहीं व्यापार असंतुलन और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गंभीर मतभेद उभरकर सामने आए। ईयू की ओर से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि चीन की ओर से सस्ते उत्पादों का निरंतर निर्यात यूरोपीय औद्योगिक संतुलन को बिगाड़ रहा है। फॉन डेय लाएन की टिप्पणी कि जैसे-जैसे साझेदारी गहरी हुई है, असंतुलन भी बढ़ा है। इस तनाव का सार है। वहीं, चीन की ओर से यह तर्क दिया गया कि कोई बुनियादी हित टकराव नहीं है और मतभेदों को संवाद से सुलझाया जाना चाहिए। इस बैठक का सबसे ठोस परिणाम दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति व्यवस्था पर बनी सहमति रहा, जो वैश्विक टेक्नोलॉजी और हरित परिवर्तन के लिए आवश्यक संसाधनों में चीन की प्रमुख भूमिका को दोहराता है। पर यह भी स्पष्ट हुआ कि चीन इन संसाधनों के नियंत्रण का रणनीतिक इस्तेमाल कर रहा है, जिससे वह यूरोप पर दबाव बना सके- विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगाए गए भारी शुल्क जैसे मुद्दों पर। रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर चीन की अस्पष्ट स्थिति एक और बड़ा रोड़ा बनी रही। ईयू का आरोप है कि चीन परोक्ष रूप से रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को समर्थन दे रहा है। वहीं, चीन ने यूक्रेन में रूस की हार को अपने हितों के खिलाफ बताया। शिखर सम्मेलन से यह भी उजागर हुआ कि यूरोपीय संघ को अपनी चीन नीति की अब पुनर्समीक्षा करनी होगी। डि-रिस्किंग और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जैसे यूरोपीय प्रयास, जो चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए हैं, बीजिंग की नजर में संदिग्ध और चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन यूरोपीय नेताओं के लिए यह संतुलन साधना आसान नहीं होगा- क्योंकि चीन यूरोपीय बाजार में अपनी पहुंच को रणनीतिक रूप से आवश्यक मानता है, विशेषकर तब जब घरेलू मांग में गिरावट और औद्योगिक अति-उत्पादन की चुनौतियां सामने हैं। इस पृष्ठभूमि में यह बैठक चीन-ईयू संबंधों में किसी बड़ी प्रगति के बजाए एक और स्थिति का आंकलन बनकर रह गई। यूरोपीय एकजुटता को बरकरार रखते हुए चीन से सटीक, संतुलित और यथार्थवादी वार्ता की आवश्यकता बनी रहेगी, जैसा कि ब्रसेल्स स्थित विशेषज्ञों ने भी दोहराया। चीन यूरोपीय एकता को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में यूरोप को अपने रुख में स्पष्टता और दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है। संक्षेप में यह शिखर सम्मेलन रिश्तों को सुधारने की बजाए यह दर्शाता है कि अब यूरोपीय संघ और चीन के बीच सहयोग की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ने की आवश्यकता है। ऐसी परिभाषा जो पारदर्शिता, पारस्परिकता और दीर्घकालिक वैश्विक स्थिरता पर आधारित हो। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन दिनों पूरी दुनिया में अलग-अलग देश टैरिफ के नाम पर अपना व्यापार बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस मामले में अमरीका सबसे आगे है। अमरीका के टैरिफ वार ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत और चीन से रिश्ते बिगाड़ कर भी वह टैरिफ वार से पीछे नहीं हट रहा है। अमरीका के टैरिफ वार का सबसे बड़ा भुक्तभोगी यूरोपीय यूनियन है, परंतु चीन के साथ हुई बातचीत में यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने बार-बार टैरिफ लगाने की बात कही। समझ से परे है कि विभिन्न देश टैरिफ बढ़ाने के नाम पर अपना व्यापार बढ़ाने में क्यों लगे हुए हैं? फिलहाल पूरी दुनिया में व्यापारिक असंतुलन बना हुआ है। अर्थ-व्यवस्था पटरी से नीचे दिख रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया में आॢथक मंदी का खतरा बरकरार है। इसलिए सभी देश अपने-अपने स्तर पर आने वाली मंदी से बचने का उपाय कर रहे हैं। खासतौर पर अमरीका जो भी कर रहा है, वह अपने व्यापारिक संतुलन को ध्यान में रखकर कर रहा है। यूरोपीय यूनियन और चीन का द्विपक्षीय वार्ता भले ही पूरी तरह सफल नहीं रहा, परंतु वह अमरीका को यह संदेश देने में सफल रहा कि अब व्यापारिक दादागिरी नहीं चल सकती। सभी देशों को एक-दूसरे की अर्थ-व्यवस्था को देखना होगा। विकसित और विकासशील देशों के बीच के अंतर को समझना होगा।
द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन