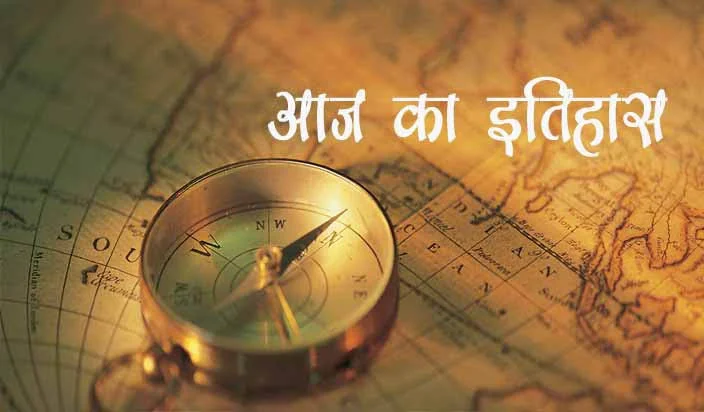चलित वर्ष 2024 की चर्चा 2023 में ही शुरू हो गई थी। खासतौर पर सियासी लोगों को इसका इंतजार बहुत पहले से था। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि सियासी घरानों और राजनीतिक रणबांकुरों को जिसका इंतजार था,वह घड़ी अब सामने आ चुकी है यानी बस दो या तीन महीने के बाद आम चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल राजनीतिक अखाड़े में बिहार में जो भी हो रहा है,वह उस राजनीतिक बेचैनी को दर्शाता है, जो जोड़-तोड़ किए बिना पूरा होता नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर खेमा बदलने जा रहे हैं, उनको अपनाने वाले खेमे को पता है कि वे पलटूराम के पद से विभूषित हैं, फिर भी वह उन्हें इसलिए अपनाने को लालायित दिख रहे हैं क्योंकि 2024 में लोग विकास के मामले में बिहार बनाम गुजरात या बिहार बनाम यूपी मॉडल पर विचार करने लगे हैं। फिलहाल बिहार मॉडल गुजरात या यूपी मॉडल पर भारी है। बिहार मॉडल में सरकारी नौकरी है तो दूसरी ओर दूसरे मॉडलों में आस्था का दोहन है और भ्रमकारी आंकड़ों से भ्रम फैलाने की पूरी कोशिश हो रही है। एक पक्ष को डर है कि यदि विकास का मॉडल कहीं बिहार बनाम यूपी या बिहार बनाम गुजरात बन गया तो सारे भेद खुल जाएंगे, इसलिए सत्ताधारी पार्टी को बिहार के मुखिया को अपने पाले में करने की जल्दबाजी दिख रही है। दूसरी ओर कागज पर भारत के पास जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले नौ वर्षों में देश में रहने वाले लगभग 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले नौ वर्षों में बहुआयामी गरीबी में 18 फीसद की गिरावट आई है। साथ ही इस स्थिति में रहने वाले लोगों की संख्या 29 फीसद से घटकर 11 फीसद हो गई है। आंकड़े दिखाते हैं कि बहुआयामी गरीबी को एक फीसद से कम करने के सरकार के लक्ष्य की दिशा में काफी प्रगति हुई है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने इन दावों के पीछे बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के उपयोग पर कुछ गंभीर संदेह उठाए हैं और कहा है कि रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो वास्तव में गरीबी की पूरी तस्वीर पेश नहीं करतीं। इन आंकड़ों की गणना का तरीका यानी कार्य प्रणाली संदिग्ध है। बहुआयामी गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर आधारित है, जिनमें से प्रत्येक को समान महत्व दिया जाता है। इन तीनों श्रेणियों को 12 संकेतकों में विभाजित किया गया है। भारत में प्रत्येक परिवार को 12 मापदंडों के आधार पर एक अंक दिया जाता है और यदि किसी परिवार का अभाव स्कोर 33 फीसद से ज्यादा है तो उसे बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में पहचाना जाता है। इसे गरीबी के स्तर और गरीबी की तीव्रता को मापने के लिए गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा विकसित किया गया था। भारत ने अपने राष्ट्रीय एमपीआई में दो नए पैरामीटर्स- मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाते भी जोड़े हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि रिपोर्ट के निष्कर्षों में गरीबी पर कोविड के विनाशकारी प्रभावों को नजरअंदाज कर दिया गया है, जबकि दूसरे विशेषज्ञों का कहना है कि इस विधि में वैश्विक स्तर पर गरीबी का आकलन करने की पारंपरिक विधि का पालन नहीं किया गया है, जिसमें उपभोग गरीबी रेखा के नीचे की आबादी की संख्या और हिस्सेदारी महत्वपूर्ण होती है। मेहरोत्रा कहते हैं कि साल 2014 और 2022 के बीच उपभोग व्यय सर्वेक्षण की अनुपस्थिति के बावजूद भारत में गरीबी संकेतक के रूप में राष्ट्रीय एमपीआई का उपयोग करना, राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। वास्तविक मजदूरी छह साल से स्थिर थी जिसका उपभोग मांगों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। जाहिर है कि गरीबी के स्तर में जो गिरावट दिखाई जा रही है, ये उसके अनुरूप नहीं हो सकती। क्या आकलन की प्रक्रिया और उसके परिणाम बारीकी से जांच करने लायक हैं? क्या एमपीआई गरीबी की पूरी तस्वीर खींचने में सक्षम है? दूसरी ओर किसी भी समग्र सूचकांक की सीमाएं होती हैं क्योंकि यह प्रभावित करने वाले कारकों की विशिष्ट पसंद के साथ-साथ उपयोग की जाने वाली पद्धति के आधार पर अत्यधिक विषम होती हैं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल बनाया जाने वाला मानव विकास सूचकांक भी वैचारिक रूप से और प्रणाली के स्तर पर आलोचनाओं से मुक्त नहीं है क्योंकि यह केवल चयनित तीन संकेतकों और प्रत्येक वैरियेबल को महत्व देने के तरीके पर आधारित है। नीति आयोग की रिपोर्ट यह भी दावा करती है कि विभिन्न सरकारी प्रयासों और कल्याणकारी योजनाओं ने विभिन्न प्रकार के अभाव को कम करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। ऐसे में सरकार की रिपोर्ट की दोबारा व्याख्या और धरातल पर इसे उतारकर इसे सही साबित करने की जरूरत है। कारण कि लोगों को आंकड़ों और शब्दों की बाजीगारी पर कम विश्वास होता है। ऐसे में विकास बहाली सबसे बड़ी जरूरत है, जिस पर भ्रम बरकरार है।
भ्रम की राजनीति