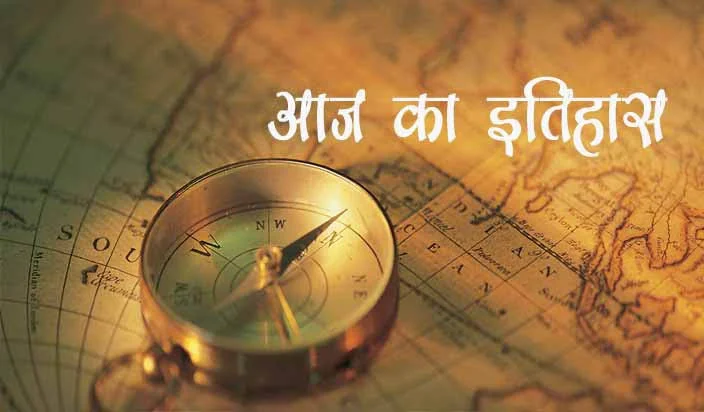गुलाम चिश्ती
आमतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों की गणना गैर-हिंदी प्रदेशों में होती है। समय-समय पर हिंदीभाषियों की हत्याएं इस मान्यता को और भी बलवती करती हैं। फिर भी, पूर्वोत्तर भारत के लोग जब अपने किसी पड़ोसी राज्य के लोगों से मिलते हैं तो उनकी संपर्क भाषा हिंदी होती है। उनके लिए हिंदी विचारों के आदान-प्रदान के लिए सबसे आसान माध्यम है। इस मामले में अंग्रेजी अब तक हिंदी की बराबरी नहीं कर पाई है। सच तो यह है कि हिंदी असम की ब्रह्मपुत्र घाटी को बराक घाटी से जोड़ती है। आज भी यहां असमिया या बांग्ला भाषा एक-दूसरे के लिए संपर्क की कड़ी नहीं बन पाई हैं, जबकि हिंदी उनके लिए सेतु का कार्य करती है। असम के दो पहाड़ी जिलों (कार्बी आंग्लांग व डिमा हसाऊ) के लोग जब गुवाहाटी, तिनसुकिया, तेजपुर या राज्य के किसी अन्य हिस्से में होते हैं तो उनकी भी संपर्क भाषा हिंदी होती है। कार्बी आग्लांग जिले के निवासी राम शरण चौहान का कहना है कि डिमा हसाऊ जिले के मुख्य शहर हाफलांग के ट्राइबल अपनी मिट्टी से रची-बसी हिंदी बोलते हैं, जिसे हाफलांगी हिंदी कहते हैं। यह दीगर बात है कि हाफलांगी हिंदी अभी तक शोध कार्यों से वंचित है। समझा जाता है कि इस पर अभी तक किसी शोध संस्था की नजर नहीं पड़ी है और यदि पड़ी भी है तो शोध पर कोई विचार नहीं किया गया। निःसंदेह हाफलांगी हिंदी को भी विस्तृत हिंदी परिवार में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे में केंद्रीय हिंदी संस्थान (आगरा) सहित राष्ट्रभाषा के प्रचार-प्रसार में जुटी संस्थाओं को अपने कार्यों में और भी सुविधा होगी। जानकारों का कहना है कि रामायण और महाभारत काल में भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब जैसे राज्यों से लोग पूर्वोत्तर में आते-जाते रहते थे। उनका यहां के लोगों के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और विवाहेतर संबंध भी स्थापित हुआ। रामायण काल के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के गुरु वशिष्ठ असम के रहने वाले थे, जिसका नमूना हम गुवाहाटी में वशिष्ठ आश्रम के रूप में देख सकते हैं।उल्लेखनीय है कि मुगल काल और अंग्रेजों के जमाने में देश की हिंदी पट्टी से लोगों का पूर्वोत्तर राज्यों में आने का सिलसिला जारी रहा। अंग्रेजों ने जब असम में चाय बागानों का विस्तार करना शुरू किया तो उस समय अविभाजित बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लोगों को यहां लाकर बसाया गया, जो अब यहां चाय समुदाय या चाय जनजाति कहे जाते हैं। उनमें से अधिकांश मूल रूप से हिंदीभाषी हैं। परंतु समय के साथ उन्होंने स्थानीय सभ्यता व संस्कृति को अपनाया और यहां की मिट्टी में रच-बस गए। आज वे वृहत्तर असमिया समुदाय के सदस्य हैं। वे सार्वजनिक तौर पर असमिया, बांग्ला, संथाली और उड़िय़ा बोलते हैं। परंतु उनकी जातीय पहचान और संस्कृति हिंदीभाषियों की तरह है। उनके उपनाम में मुंडा, उरांव, मांझी, सिंह, घटोवार, धनोवार, कुर्मी, मल्लाह, ग्वाला और तेली जैसे शब्द लगाए जा रहे हैं। वे अपने घरों में झारखंड और बिहार की लोकभाषाओं का उपयोग करते हैं। आज हाट-बाजार, बस अड्डों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, नाई व धोबी की दुकानों की भाषा हिंदी है। यदि किसी सफाई मजदूर को आमंत्रित करना है तो उसके लिए भी हिंदी की जरूरत है। यदि रिक्शा चालक और दैनिक मजदूरों से बात करनी है तो हिंदी के बिना काम नहीं चल सकता। उल्लेखनीय है कि गुवाहाटी सहित राज्य के विभिन्न इलाकों में कार्यरत नाई, धोबी और सफाई मजदूरों में अधिकांश हिंदीभाषी हैं। एक दलित नेता का कहना है कि हमारे पूर्वज बहुत पहले बिहार के गोपालगंज जिले से असम आए थे। आज हमारे काफी लोग सफाई मजदूर के रूप में यहां कार्यरत हैं। हम यहां के जनजीवन में पूरी तरह घुल-मिल गए हैं और अब असमिया भाषा, सभ्यता व संस्कृति हमारी पहचान है। हम वृहत्तर असमिया संस्कृति के अंग हैं। बावजूद इसके, हम अपने परिजनों के साथ हिंदी और भोजपुरी में भी बात करते हैं। गुवाहाटी के लाचित नगर में धोबी का काम करने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि उसके पूर्वज भी बिहार के गोपालगंज से आए थे, परंतु अब गुवाहाटी ही अपना सब कुछ है। राज्य में जब से भाजपा सरकार आई है तब से यहां हिंदी भाषा को विशेष महत्व मिल रहा है।