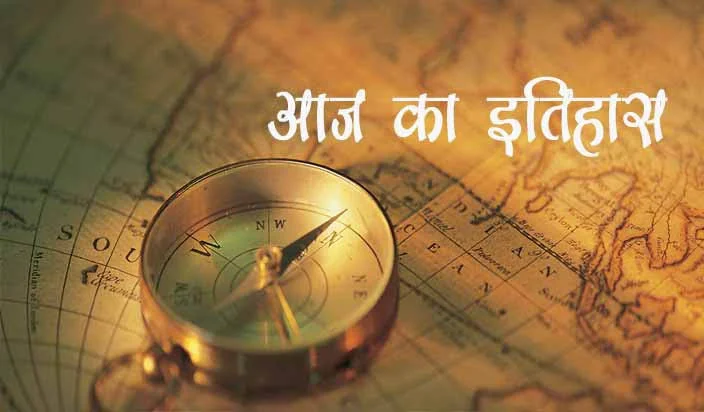जलवायु परिवर्तन पर कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें संस्करण यानी कॉप 28 की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। कॉप शिखर बैठकों का मूल उद्देश्य ऐसे बाध्यकारी समझौतों को अंजाम देना था जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने में मदद करे। जानकार बताते हैं कि ग्रीनहाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं, इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाई ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरो-फ्लोरो कार्बन, वाष्प और ओजोन आदि करती हैं। कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन पिछले 10-15 सालों में 40 गुणा बढ़ गया है। दूसरे शब्दों में औद्यौगिकीकरण के बाद से इसमें 100 गुणा की बढ़ोत्तरी हुई है, इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरणों वातानुकूल, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर और कार आदि से होता है। कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत पेट्रोलियम ईंधन और परंपरागत चूल्हे हैं। पशुपालन से मीथेन का उत्सर्जन होता है। कोयला बिजली घर (यानी पॉवर हाउस) भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत हैं। हालांकि क्लोरोफ्लोरो का प्रयोग भारत में बंद हो चुका है, लेकिन इसके स्थान पर प्रयोग हो रही गैस हाइड्रो क्लोरो-फ्लोरो कार्बन सबसे हानिकारक ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाई ऑक्साइड की तुलना में एक हजार गुना ज्यादा हानिकारक है। कार्बन डाई ऑक्साइड गैस तापमान बढ़ाती है।
उदाहरण के लिए वीनस यानी शुक्र ग्रह पर 97.5 प्रतिशत कार्बन डाई ऑक्साइड है जिस कारण उसकी सतह का तापमान 467 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में पृथ्वीवासियों के लिए राहत की बात यह है कि धरती पर उत्सर्जित होने वाली 40 प्रतिशत कार्बन डाई ऑक्साइड को पेड़-पौधे सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन उत्सर्जन करते हैं। उल्लेखनीय है कि पेरिस समझौते के बाद के दौर में इसमें काफी बदलाव आया है। अब ऐसी शिखर बैठकों की उपयोगिता इस बात के इर्द-गिर्द तय होती है कि क्या वहां उपस्थित नेताओं को साझा लक्ष्य तय करने की दिशा में ले जाया जा सकता है,भले ही वे कानूनी रूप से बाध्यकारी न हों। कॉप में ऐसे दो लक्ष्य घोषित किए गए। इनके अलावा जलवायु और स्वास्थ्य को लेकर एक व्यापक समझौता हुआ। वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 2030 तक तीन गुना करने के लक्ष्य को 20 देशों का समूह अपने नई दिल्ली घोषणापत्र में ही आगे बढ़ा चुका है। नाभिकीय ऊर्जा संबंधी घोषणा खासतौर पर दिलचस्प है। आंशिक तौर पर इसलिए कि हरित ऊर्जा बदलाव में नाभिकीय ऊर्जा की भूमिका का विरोध देखने को मिला है। यहां तक कि यूरोपीय संघ के भीतर भी दो प्रमुख शक्तियों फ्रांस और जर्मनी का नजरिया इस विषय पर एकदम अलग-अलग है।
पूर्व चांसलर एंगेला मर्केल के नेतृत्व में जर्मनी ने एक दशक से भी अधिक पहले अपने नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों को बंद करना आरंभ कर दिया था। इस बीच फ्रांस अभी भी ऊर्जा उत्पादन के लिए काफी हद तक नाभिकीय ऊर्जा पर भरोसा करता है। जर्मनी का रुख कई पर्यावरण कार्यकर्ताओं के अनुरूप है जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बुनियादी तौर पर असुरक्षित मानते हैं, परंतु यह स्पष्ट है कि दलील का यह पहलू सैद्धांतिक रूप से कमजोर है। अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय ऊर्जा एजेंसी ने कॉप-28 में कई देशों के साथ एक वक्तव्य तैयार किया जिसने स्पष्ट किया कि विशुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए नाभिकीय ऊर्जा की आवश्यकता है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में इजाफा किए बिना उत्सर्जन में कमी का कोई लक्ष्य हासिल नहीं होगा। इसलिए भारत पर भी कोयला के खनन और उत्पादन और कोयला आधारित बिजली के उत्पादन को कम करने का दबाव है। आज भी वर्षों से बंद पड़े संयंत्रों और सीमित निवेश के बाद 30 देशों में करीब 400 नाभिकीय रिएक्टर अभी भी दुनिया की कुल बिजली का 10 फीसदी उत्पादित कर रहे हैं और दुनिया के कम कार्बन वाले उत्पादन में उनकी हिस्सेदारी 25 फीसदी है।