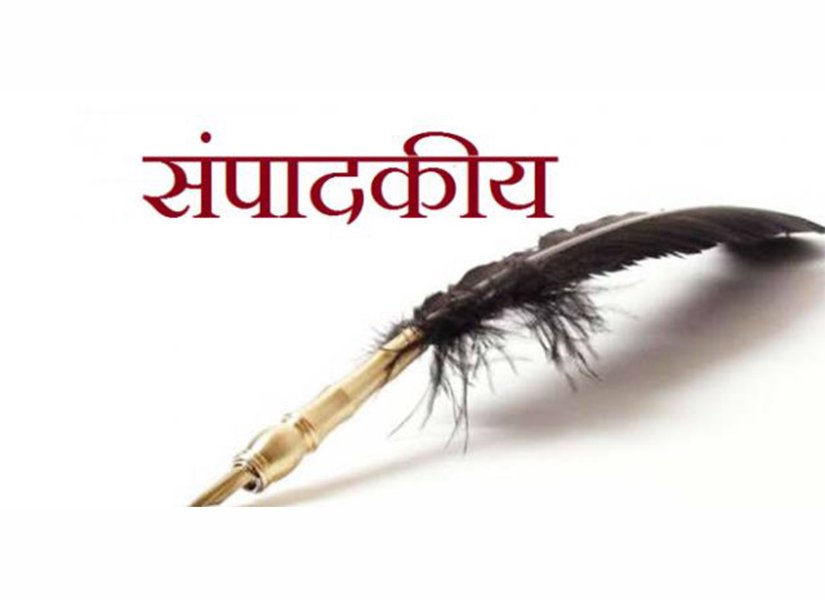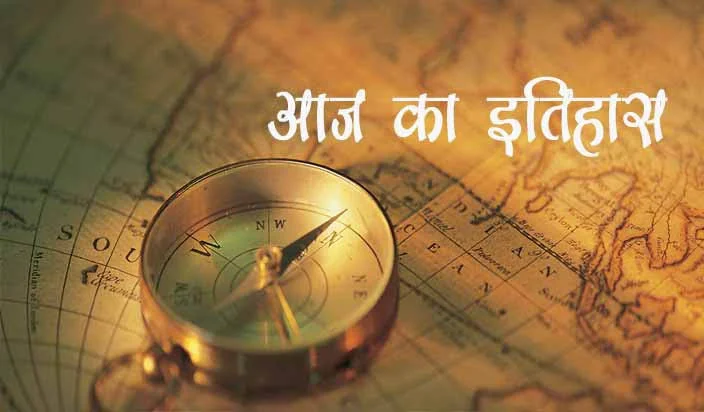भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत ने 2022 में 17.86 मिलियन टन नॉन-बासमती चावल का निर्यात किया था, जिसमें 10.3 मिलियन टन नॉन-बासमती सफेद चावल भी शामिल है, परंतु सितंबर 2022 में भारत ने बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया और चावल की अलग अलग किस्म के निर्यात पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाया था। उल्लेखनीय है कि भारतीय किसान साल में दो बार धान की रोपाई करते हैं। इस फैसले के बाद भारत जितना चावल निर्यात करता है अब वो करीब करीब आधा हो जाएगा। भारत सरकार के इस फैसले से दुनिया भर के खाद्य बाजार में चावल के दाम बढऩे की आशंका है, जबकि आजादी के तुरंत बाद के दौर में भारत खाद्यान्न के मामले में काफी गरीब रहा। हालांकि आज भारत अपने बड़े निर्यातक के दर्जे पर काफी गर्व करता है। बदलती सच्चाइयों के बीच यह गर्व नहीं चिंता की बात लगने लगी है।
इसकी मुख्य वजह है- पानी। पानी चावल यानी धान की खेती में बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। चावल या ऐसी ही अन्य फसलों में उन फसलों की शक्ल में छिपकर असल में देश का भूजल निर्यात हो रहा होता है। पानी के इस छिपे हुए निर्यात को वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट कहा जाता है। भूजल के मामले में पहले से ही गरीब भारत से यह वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट लगातार जारी है। साल 2021 को छोड़ दें तो साल 2017 के बाद से लगातार चीन ने चावल के उत्पादन में कमी की है। मिस्र खेती के अपने स्रोतों का पूरा इस्तेमाल नहीं करता और अपने खाद्य उत्पादन का करीब 40 फीसदी आयात करता है। हाल ही में थाईलैंड ने अपने किसानों से चावल के बजाए पानी के कम इस्तेमाल वाली फसलों की खेती करने को कहा है।
दूसरी तरफ बीच के दो एक सालों को छोड़ दें तो भारत से चावल का निर्यात 2016 के बाद से लगातार बढ़ा है, बल्कि 2016 से तुलना करें तो 2022 में यह दोगुना हो गया था। इस मामले में बारीकी से देखें तो भारत सिर्फ चावल नहीं बल्कि चावल उगाने में भारी मात्रा में इस्तेमाल होने वाले भूजल का भी निर्यात कर रहा है और यह संकट लगातार बढ़ रहा है, इसकी वजह है गेहूं और चावल जैसी फसलों के बड़े निर्यातक, भारत की इन फसलों की खेती के लिए भूजल पर निर्भरता का और बढ़ते जाना है। आज भारत साल भर में कुल मीठे पानी का जितना इस्तेमाल करता है, उसका 80 फीसदी सिर्फ खेती में इस्तेमाल होता है। वाटर रिसोर्सेज ग्रुप के मुताबिक भारत के पास अपनी जरूरत का सिर्फ 50 फीसदी पानी होगा। यह खतरा अब टाला नहीं जा सकता और खेती पर इसका बहुत बुरा असर होना तय है। अनियमित बारिश के बीच किसानों के लिए फसलें उगाने के लिए भूजल ही स्थायी स्रोत होते हैं। कुछ इलाकों में नहरों से सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन देश के बहुत से इलाकों में इसकी सुचारू व्यवस्था नहीं है। बिहार के बेतिया और सासाराम जैसे सीमावर्ती जिलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए बारिश के भरोसे भी रहना संभव नहीं होता। ऐसे में इलाके के ज्यादातर किसान ट्यूबवेल से सिंचाई करते हंै और कई बार खरीदे हुए पानी से सिंचाई करनी होती है। खेतों की समुचित सिंचाई सिर्फ समृद्ध किसानों के लिए ही संभव हो पाती है। वंचित जातियों के लोगों के पास जो थोड़े बहुत खेत हैं, वो उनकी सिंचाई का भी प्रबंध नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित बिहार के कुछ जिलों के किसान बताते हैं कि धान की फसल के लिए कुछ हद तक बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है, नहीं तो पूरी तरह से डीजल इंजन से सिंचाई करना इतना महंगा पड़ेगा कि खेती से कमाई के बजाए घाटा होगा। बारिश के अनिश्चित पैटर्न के बीच भूजल से सिंचाई की परंपरा पिछले दो दशकों में ज्यादा बढ़ी है। सिंचाई के मामले में सिंचाई के लिए पानी की फिजूलखर्ची भी है। दुनिया भर में सामान्य कृृषि उपज के लिए जितना पानी इस्तेमाल होता है, उत्तर प्रदेश में उतनी ही उपज के लिए दो से तीन गुना पानी इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर पानी की फिजूलखर्ची से बचने की जरूरत है।